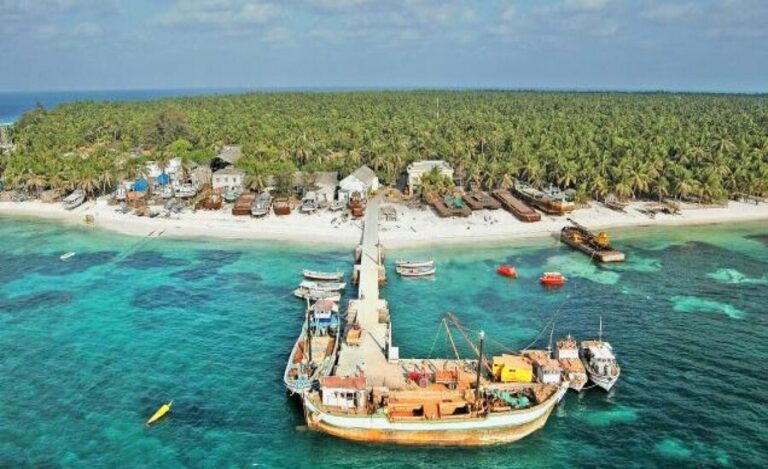इस लेख में आप पढ़ेंगे: Article 143: सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार/ Advisory Jurisdiction- UPSC
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने Article 143 के तहत किए गए 16वें राष्ट्रपति संदर्भ पर अपनी राय दी है। अपनी राय में सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 2025 में दिए गए दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को काफी हद तक नकार दिया है।
राष्ट्रपति का संदर्भ क्या था? Presidential Reference
वर्तमान संदर्भ अप्रैल 2025 में तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का परिणाम है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रगतिशील फैसला सुनाया था:
- राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की गई थी।
- न्यायालय ने कहा कि ऐसे विधेयकों पर राज्यपालों और राष्ट्रपति के निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
- न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित उन विधेयकों को ‘मान्य स्वीकृति‘ (Deemed Assent) प्रदान की, जिन पर राज्यपाल की सहमति बहुत समय से लंबित थी।
वर्तमान संदर्भ में न्यायालय की राय हेतु 14 प्रश्न उठाए गए थे, जिनमें मुख्यतः अनुच्छेद 200 और 201 की व्याख्या शामिल थी। ये प्रश्न न्यायालयों के उस अधिकार से संबंधित हैं जिसके तहत वे समय-सीमाएँ निर्धारित कर सकते हैं, जो संविधान में कहीं भी निर्दिष्ट नहीं हैं। सरकार ने प्रश्न किया था कि क्या राज्यपालों और राष्ट्रपति के कार्यों को किसी विधेयक के कानून बनने से पहले ही न्यायिक समीक्षा के अधीन लाया जा सकता है। संदर्भ में Article 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली शक्तियों की सीमा पर भी राय मांगी गई थी।
वर्तमान राय क्या है? (Advisory Jurisdiction)
सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की पीठ ने उठाए गए प्रश्नों पर अपनी राय दी है। पीठ ने कहा कि यह संदर्भ एक ‘कार्यात्मक संदर्भ‘ है, जो संवैधानिक पदाधिकारियों के दैनिक कामकाज और राज्य विधानमंडल, राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच परस्पर संबंधों की समीक्षा मांगता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न उत्तर दिए हैं:
- जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास तीन संवैधानिक विकल्प होते हैं: अनुमति देना, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना, या अनुमति रोक लेना और विधेयक को टिप्पणियों के साथ विधानमंडल को वापस करना।
- राज्यपाल को इन तीन विकल्पों में से चुनने का विवेकाधिकार प्राप्त है और वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य नहीं है।
- अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा कार्यों का निर्वहन न्यायोचित (न्यायिक समीक्षा के अधीन) नहीं है, लेकिन लंबे समय तक अस्पष्टीकृत निष्क्रियता की परिस्थितियों में, न्यायालय राज्यपाल को प्रस्तुत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए एक सीमित परमादेश (Limited Mandamus) जारी कर सकता है।
- संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा के अभाव में, न्यायालय न्यायिक रूप से राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा कार्रवाई के लिए समयसीमा निर्धारित नहीं कर सकता है।
- अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति/राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों का स्थान नहीं ले सकतीं। इसलिए, विधेयकों पर ‘मान्य स्वीकृति’ (deemed assent) की अवधारणा की कोई अनुमति नहीं है।
इस राय से सम्बंधित समस्याएं:
- संघवाद पर आघात: यह राय राज्यपालों को संवैधानिक जवाबदेही के बिना राज्य के कानूनों को अवरुद्ध करने या विलंबित करने की अनियंत्रित शक्तियाँ प्रदान करता है।
- न्यायालय ने समय-सीमा और अनुच्छेद 142 के प्रयोग को अस्वीकार करने के लिए शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत (Separation of powers) का सहारा लिया, लेकिन यह निर्णय राज्य के अधिकारों की कीमत पर राज्यपालों को अधिक सशक्त बनाता है। निर्णय में दावा किया गया है कि अनुच्छेद 200 और 201 कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं करते। परन्तु अनुच्छेद 200 में स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल को अपना निर्णय “यथाशीघ्र” घोषित करना होगा – न्यायालय के अनुसार, यह संवैधानिक भाषा ‘अस्पष्ट‘ होने के कारण समयसीमा का समर्थन नहीं करती है। पुंछी आयोग (2010) ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल को अपनी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत विधेयक पर छह महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए। के. एम. सिंह मामले (2020) में न्यायालय ने अपने ही फैसले में, अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए अध्यक्षों के लिए तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की थी, हालाँकि संविधान में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। तमिलनाडु राज्य मामले में राज्यपालों और राष्ट्रपति को समय-सीमा प्रदान करने का फैसला संविधान की एक उद्देश्यपूर्ण और प्रगतिशील व्याख्या थी। वर्तमान मत ने इस स्थिति को नकार दिया है।
- राज्यपाल की बढ़ती विवेकाधीन शक्ति से लोकतांत्रिक जनादेश कमजोर होता है: न्यायालय का यह दावा कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य नहीं हैं, संवैधानिक इतिहास का खंडन करता है। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 200 और 201 से “अपने विवेकानुसार” (1935 के अधिनियम में प्रयुक्त वाक्यांश) को स्पष्ट रूप से हटा दिया था। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति को सीमित करते हुए सरकारिया आयोग (1987) ने कहा था कि केवल राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों का आरक्षण (वह भी स्पष्ट रूप से असंवैधानिक मामलों में) ही राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति माना जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने शमशेर सिंह (1974) और नबाम रेबिया (2016) सहित विभिन्न मामलों में यह माना था कि राज्यपालों को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए। वर्तमान राय इन संवैधानिक मिसालों को उलट देती है। इससे जनता द्वारा निर्वाचित राज्य सरकारों की विधायी मंशा पटरी से उतरने की संभावना है।
- न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि स्वीकृति रोकने के बाद विधेयक को विधानसभा में वापस भेजना होगा। लेकिन निर्णय में यह भी कहा गया है कि यदि विधानसभा विधेयक को दूसरी बार भी पारित कर देती है, तो भी राज्यपाल के पास इसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखने का विकल्प सुरक्षित रहता है। इससे विधानमंडल द्वारा दूसरी बार पारित किए जाने की बाध्यकारी प्रकृति समाप्त हो जाती है। परिणामस्वरूप, चाहे पहली बार में या पुनर्विचार के बाद, राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। एक बार वहां जाने के बाद, विधेयक अनिश्चित काल तक लंबित रह सकते हैं क्योंकि निर्णय में कहा गया है कि राष्ट्रपति का न्यायालय से परामर्श करने का कोई दायित्व नहीं है। विधानसभा के पास विधेयकों को बाध्यकारी तरीके से दोबारा पारित करने का कोई विकल्प नहीं है, और निर्णय में इस बारे में कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास कब भेजना उचित है।
- हालाँकि यह निर्णय लंबे समय तक निष्क्रियता के लिए “सीमित परमादेश” की बात करता है, लेकिन यह “उचित समयावधि” को परिभाषित करने से इनकार करता है, जिससे राज्यों को देरी साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है।
प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों (समयसीमा और मान्य सहमति), असाधारण उपायों (अनुच्छेद 142), और निरीक्षण (अनुच्छेद 200 के तहत कार्यों की न्यायिक समीक्षा) को हटाकर, न्यायालय की राय ने कार्यपालिका के अतिक्रमण की संभावना को बढ़ावा दिया है। राज्यों के पास मनमाने विलंब को चुनौती देने के लिए बहुत कम तंत्र बचते हैं। हमारी संघीय व्यवस्था को ग्रसित करने वाली मूल बीमारी राज्यपाल पद का राजनीतिकरण रही है। राज्यपाल राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए केंद्र द्वारा नियुक्त व्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं। हालाँकि, संघवाद भी हमारे संविधान की एक मूलभूत विशेषता है। सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान राय राज्यपाल द्वारा राज्यों में लोकप्रिय रूप से निर्वाचित सदनों की नीतियों को विफल करने का बहाना नहीं बननी चाहिए। राज्यपालों को राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने में ज़िम्मेदार तत्परता दिखानी चाहिए।